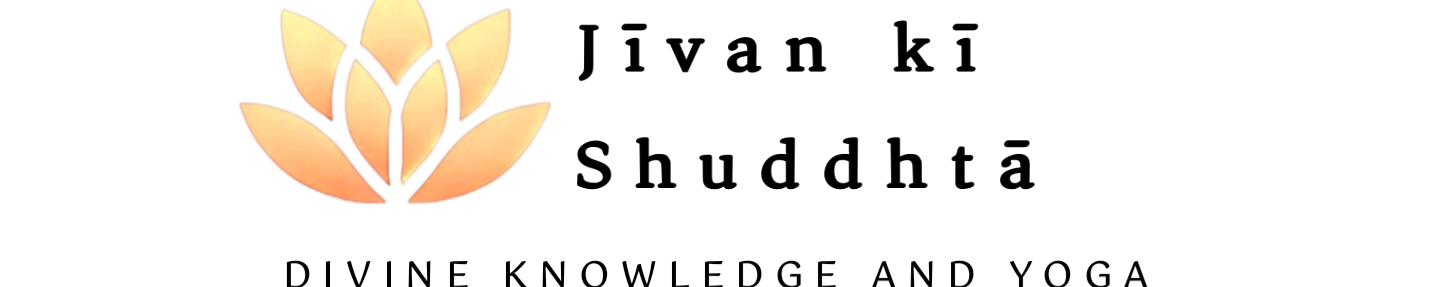कर्मयोग – श्रीमद भागवत गीता
नमस्कार साधकों!
कर्मयोग क्या है?
क्या केवल बिना फल की चिंता किए कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मयोगी कहलाता है?
क्या कर्मयोग के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है?
भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग का उपदेश दिया था।
उन्होंने कहा, “हे अर्जुन! तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मफल के हेतु मत बनो, और न ही “अकर्मण्यता” यानी कर्म न करने में आसक्त होओ।”
युद्धभूमि में अर्जुन भावनाओं में बहकर युद्ध से निकलने वाला था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए युद्ध की आवश्यकता बताई जो उसका कर्म है, और यह भी कहा की तुम केवल युद्ध करों, हारने या जितने, पाने या खोने, जीवित रहने या मरने से ऊपर उठो। और अपना कर्तव्य करो जो की केवल युद्ध करना मात्र है। उसमे हारना या जितना भी नहीं,
साधकों! यह बात सुनने में सरल लगती है, पर इसे समझना और अपने जीवन में उतारना ज्यादातर लोगों के लिए अत्यंत कठिन है।
ज्यादातर सामान्य लोग, जो योगी नहीं हैं, कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म अक्सर स्वार्थ, अहंकार और इच्छाओं से बंधे होते हैं।
जब हम फल और परिणाम की आशा से कर्म में लगे होते हैं, तो हम स्वयं को बंधन में जकड़ लेते हैं, जो आत्मा की पवित्रता से वियोग का कारण बनता है।
जो जीव है उनके सारे कर्म किसी न किसी निजी लाभ या स्वार्थ के लिए होते हैं, वे स्वयं को हमेशा पूर्ण करना चाहते है।
जैसे, यदि किसी को खाने का बहुत शौक है और वह खाली बैठा है, तो वह कुछ न कुछ पकाने में लग जाता है। यह उसकी इच्छा है जो उसे कर्म की ओर प्रेरित करती है।
इसी प्रकार, हम कोई भी कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसके परिणाम की अपेक्षा होती है। लेकिन जब ऐसा करते हैं, तो चेतना, जो निस्वार्थ और पवित्र है, स्वार्थ, अहंकार की परतों में ढक जाती है।
जैसे एक शांत झील का पानी स्वच्छ और निर्मल होता है, लेकिन अगर उसमें कोई व्यक्ति कूद पड़े, तो पानी गंदला हो जाता है और उसका वास्तविक स्वरूप बदल जाता है।
उसी प्रकार, चेतना का मूल स्वभाव भी निस्वार्थ और शुद्ध होता है वह अकर्ता है , लेकिन जब स्वार्थ, अहंकार और इंद्रियतृप्ति की लालसा उस पर हावी हो जाता है, तो वह मलिन हो जाता है, जो योग की सिद्धि के विपरित दिशा में ले जाता।
कर्ताभाव यानी “मैं कर्ता हूं यह मान्यता” यह वह भावना है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम स्वयं कर्ता हैं।
यह सोच जीव को कर्म के बंधन में बाँध देती है। लेकिन वास्तव में, जीवों का स्वरूप यानी की चेतना कर्ता नहीं हैं, बल्कि भौतिक शरीर कर्ता है जो जीव का स्वरूप नहीं है।
साधकों!
जैसे कोई व्यक्ति किसी यंत्र पर सवार होकर उसे नियंत्रित करता है, वह उस यंत्र के माध्यम से ऐसे-ऐसे कार्य करता है जो बिना यंत्र के असंभव होते हैं।
उस स्थिति में, कर्ता वह व्यक्ति नहीं, बल्कि वह यंत्र होता है, जो कार्य को संपन्न करता है।
उसी प्रकार, संसार में जो भी कार्य होते हैं, वे हमारे शरीर और उसकी ऊर्जा से होते हैं,
न कि चेतना से वह पवित्रता तो बस साक्षी है, वह केवल दृष्टा है, वह न तो कुछ करता है और न ही किसी फल की आकांक्षा में है।
अगर यंत्र पर सवार व्यक्ति अपनी पहचान भूल जाए और स्वयं को यंत्र ही मान ले, तो वह स्वयं को कभी यंत्र से अलग कर नहीं पाएगा और स्वयं को उस यंत्र बंधनों में बाँध लेगा।
उसी प्रकार, यदि साधक अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को शरीर, इंद्रियां और मन मान लेता है, तो वह कर्मों के जाल में फँस जाता है। चेतना के वास्तविक स्वरूप को बदल देगा।
कर्मयोग यानी की कर्म करते हुएं योगारूढ़ स्थिति में रहना, यानी कि कर्म करते हुए भी स्वयं को कर्म से अछूता रखना।
यह जानना कि ‘मैं’ कर्ता नहीं हूँ, बल्कि यह शरीर और इसकी ऊर्जा कर्म कर रहे हैं। मैं अकर्ता और सभी बंधनों से परे विशुद्ध चैतन्य मात्र हूं।
जब साधक इसका साक्षात्कार कर लेता है, तब वह कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त रहता है, यानी वह कर्मयोगी होता है, जो कर्म को मुक्ति तक का साधन बना लेता है।
कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना है। यह योग का वह उच्चतम स्वरूप है जिसमें साधक कर्म करते हुए भी मोक्ष की ओर ही बढ़ता है।
कर्म करना हमारे जीवन का स्वभाव है, उससे हम बच नहीं सकते, हर व्यक्ति हर जीव इस संसार में कर्म से बंधा होता हैं।
लेकिन वह कर्मयोगी कर्म करते हुएं भी चेतना के वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है जो नित्य शांति देता है
कर्म करते हुएं भी उसके बंधन में न बंधे – यही कर्मयोग का मर्म है।
कर्मयोग का अभ्यास हमें आत्मा के निस्वार्थ और शुद्ध स्वरूप की ओर ले जाता है, जहाँ मोक्ष है।
——-
पुराने समय की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहते थे। वह अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन, उनके पास एक व्यापारी आया, जो अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसने संत से पूछा, “गुरुदेव, मैं जीवन में अनेक कर्म करता हूँ, लेकिन शांति मुझे कभी नहीं मिलती। कृपया मुझे कर्मयोग क्या है और इससे शांति पाने का रहस्य समझाइए।”
संत ने मुस्कुराते हुए कहा, “कल तुम मेरे साथ आश्रम के बाग में आना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा।”
अगले दिन, व्यापारी बाग में पहुँचा। संत ने उसे एक बाल्टी दी और कहा, “इन सूखे पत्तों को उठाकर उस गड्ढे में डाल दो।” व्यापारी ने पूरे मन से पत्तों को उठाना शुरू किया। जब वह गड्ढे के पास पहुँचा, तो हवा का एक तेज़ झोंका आया और कुछ पत्ते वापस बिखर गए।
व्यापारी को गुस्सा आया और वह पत्तों को फिर से इकट्ठा करने लगा। जैसे ही वह उन्हें डालने गया, फिर से हवा आई और पत्ते उड़ गए। यह सिलसिला कई बार चला। थक-हारकर व्यापारी संत के पास पहुँचा और कहा, “गुरुदेव, यह कार्य तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। हवा बार-बार मेरे परिश्रम को व्यर्थ कर देती है।”
संत ने शांत स्वर में कहा, “यही तो जीवन का सच है। जब तक तुम परिणाम को अपने मन में रखकर कर्म करोगे, तब तक तुम्हें दुख और क्रोध मिलेगा। यदि तुम इन पत्तों को सिर्फ कर्म समझकर उठाते और हवा के उड़ाने पर भी शांत रहते, तो तुम्हें शांति मिलती। ऐसा करते हुएं तुम स्वयं को कर्म बंधन के दोषों से मुक्त रखते ही हों और स्वयं को एक योगी भी बनाते हों।
संत ने आगे समझाया, “कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए योग अभ्यास करना।
जैसे हवा पत्तों को उड़ा रही है, वैसे ही संसार में अनेक शक्तियाँ हैं जो हमारे कर्मों के परिणामों को प्रभावित करती हैं। अगर हम परिणाम पर अधिकार जताएंगे, तो हमें दुःख ही मिलेगा।”
उस संत ने यह भी बताया की इस संसार में जो पैदा होता है यह प्रकृति उसे किसी न किसी कर्म से बांध देती है , चाहें वह एक सिद्ध योगी या कोई साधारण जीवात्मा, लेकिन एक कर्मयोगी कर्म करते हुएं भी उसके परिणाम से अलग होता है। वह कभी नहीं सोचता की मेरे कर्म का क्या परिणाम होगा क्या मुझे लाभ होंगा या हानि, मेरी समय और ऊर्जा भी व्यर्थ न हो जाएं, इसलिए वह स्वाभाविक वहीं कर्म करता है जो उसका धर्म है।
व्यापारी की आँखें खुल गईं। वह समझ गया कि उसे कर्म तो करना है, लेकिन उस कर्म को एक बंधन बनाएं बिना उसने संत को प्रणाम किया और शांति का अनुभव करते हुए अपने घर लौट गया।
तो साधकों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म तो अनिवार्य हैं, लेकिन उनसे बंधे रहना हमारी अंतरिक अशांति और आत्म के पवित्रता से वियोग का कारण है।
तो साधकों,
कर्मयोग का सार यही है – कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना। अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी, कर्ताभाव से अच्छे और बुरे दोनों परिणामों से मुक्त हो जाना।
जब हम समझ जाते हैं कि हम केवल साक्षी हैं, और कर्म तो इस भौतिक शरीर और इसकी ऊर्जा से हो रहे हैं, तब हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही कर्मयोग का उच्चतम स्वरूप है।
तो आइए, हम भी अपने जीवन में कर्मयोग का अभ्यास करें।
फल और परिणाम से जुड़े बिना अपने कर्तव्यों को निभाएं और आत्मा के शुद्ध, निस्वार्थ स्वरूप में स्थित रहें।
आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।
तब तक के लिए, ध्यान, साधना और कर्मयोग के पथ पर अग्रसर रहें।
धन्यवाद!